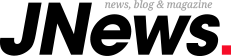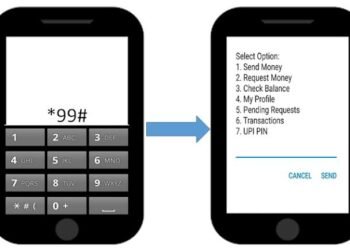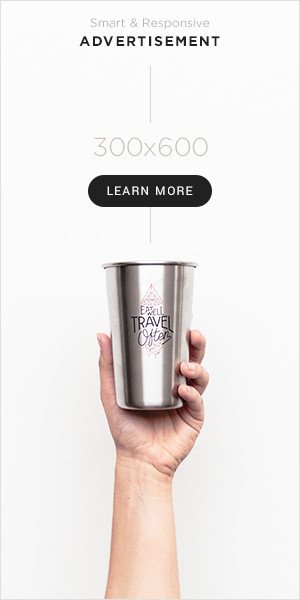कहाँ जाऊँ, दिल्ली या उज्जैन ?
 मेरा सिर गरम है
मेरा सिर गरम है
इसीलिये भरम है
सपनों में चलता है आलोचन
विचारों के चित्रों की अवलि में चिन्तन।
निजत्व- भाप है बेचैन,
क्या करूँ, किससे कहूँ
कहाँ जाऊँ, दिल्ली या उज्जैन ?
मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता ‘अँधेरे में’ की ये पंक्तियां कवि के किस संशय को प्रकट करती हैं? इस कविता को 1957 से 1962 के बीच नागपुर-राजनांदगांव में रचते हुए, बावड़ियों और खोहों में व्याप्त अँधेरे की गहन पड़ताल करते हुए कवि के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ होगा। अपनी प्रकृति में नितान्त विपरीत दो छोरों के बीच झूलते मन के समक्ष अपने समय का बेहद व्याकुल प्रश्न!
कुछ सूझता नहीं कि अपने जीवन के 42 वर्षों के व्यतीत में किसे ‘अपना जनपद’ कहूँ और किन्हें ‘अपने लोग’! उज्जैन, जहाँ जन्म के साथ अपने जीवन के 25 वर्ष कपूर की तरह उड़ गये, भोपाल, जहाँ कविता में आँखें खुली, इन्दौर, जहाँ नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में जीवन को अलग तरह से समझना शुरू किया या फिर गुना, जो एक नियति है, एक ठोस वर्तमान! और फिर ये ही क्यों –दिल्ली, नागपुर या महिदपुर क्यों नहीं? कौन नहीं है अपना, अपना-सा! यह मुश्किल सवाल अपने आप में बहुत सुखद है। इस संशय को प्यार करने का मन हो आता है, सहज ही।
लेकिन चूंकि बात मुक्तिबोध से प्रारम्भ की है तो पाता हूँ कि जीवन के क्रूरतम यथार्थ की अभिव्यक्ति करते समय यह संशय सियासत की कड़वी सच्चाईयों के केन्द्र और शहर होने की कोशिश करते एक ठेठ मालवी कस्बे के बीच चुनाव की कोई रचनात्मक कोशिश रही होगी। सम्भव है उस समय कवि के मन में कालिदास के ‘मेघदूत’ के शापित यक्ष रहा हो जो धूल और धुएं के वायवीय बादल को यह सूत्र दे रहा हो –
‘ वक्रःपन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां ’
उज्जैन के चुम्बकत्व से मुक्ति असंभव है बन्धु ! इस शहर में यह चुम्बकत्व एकांगी नहीं है–याने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच के आकर्षण के साथ ही दक्षिणी-दक्षिणी ध्रुवों का विकर्षण भी है–याने कि पूर्ण चुम्बकत्व! महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग, मेले-ठेले,दाल-बाफले और भांग से युक्त एक अलसायी और मस्त-सी ज़िंदगी! लेकिन फिर भी उतनी ही आकर्षक और जीवन्त जितना कि जीवन को होना चाहिये।
मालवा की इस धीर-गम्भीर धरा में अब डग-डग पर रोटी और पग-पग पर नीर भले ही न मिले एक तरल आत्मीयता से सराबोर समय हमेशा उपस्थित मिलेगा। आत्मीय समय जिसने एक आत्मीय समाज रचा है।
कठिन-से कठिन समय और उसे यूं ही हवा में उड़ा देने की उज्जैनी युक्ति–‘ ओ भिया, फिकर नाट!’ गम्भीर क्विक मार्च, गगन में कर्फ्यू और धरती पर चुपचाप जहरीली छीः थूः के बीच वहीं कहीं माधव कॉलेज का अहाता है जहाँ बैठ कर मुक्तिबोध बीड़ी सुलगाते हैं।
सीन बदलता है– घण्टाघर! शहर के बीचों-बीच खड़ा एक दैत्याकार भवन जो शहर को अच्छे-बुरे समय का पता दे रहा है। इन दिनों सफेद झक्क…! आसपास अत्याधुनिक मार्केट,मुम्बई के चौपाटी जैसी शाम……बदलते परिवेश में ‘टॉवर’ की संज्ञा पाकर इतराता-सा! मुक्तिबोध के ज़माने में गेरुए रंग से पुता, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुम्बद जहाँ सांवली हवाओं में काल टहलता है।
मुक्तिबोध से सीधे चलें कथाकार नरेन्द्र नागदेव के यात्रा वृत्तान्त ‘रोम से रोम तक फैला यूरोप’ के पास! लिखते हैं—‘पेरिस की आर्क डि ट्रम्फ दुनिया की सबसे फैशनेबल सड़क है। फैशन…परिधान…रंगीनियां…उन्मुक्तता…’ अचानक याद आ जाता है नरेन्द्र को 1960-70 के उज्जैन का घण्टाघर जब ‘अलका शर्मा और उसकी एक सहेली स्कर्ट पहन कर साइकिल चलाते हुए निकल गई थी तो घण्टाघर हिल गया था और कनछेदी की दुकान पर पान खाते लोगों के मुँह खुले रह गये थे…. नहीं आर्क डि ट्रम्फ दुनिया की नम्बर दो फैशनेबल सड़क हो सकती है, नम्बर वन नहीं।’
छठवीं कक्षा का विद्यार्थी रहा हूँगा। सरकारी स्कूल, जो एक धर्मशाला में लगता था। प्रति शुक्रवार को सरस्वती पूजन होता। चने-चिरौंजी का प्रसाद बंटता और फिर गीत वगैरह गाये जाते। साहित्यिक -सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर यही था जहाँ से कुछ लिया जा सकता था। हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे– कमलकान्त पण्ड्या। एक शुक्रवार को उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी पाठ्य पुस्तक में से ‘एक घड़े की कविता’ का सस्वर, अभिनय पाठ करने का निर्देश दिया। सिखाया भी कि कैसे करना है। कविता ऐसी थी कि एक घड़ा है जिसे ‘कुटिल कंकड़ों’ से मांज-मांज कर, रस्सी का फंदा पहना कर कुएं में उतार दिया गया है जहाँ वह कुएं की दीवारों से टकरा रहा है, ‘डुबुक’ की ध्वनि के साथ सप्रयास पानी में डुबोया जा रहा है। अंततः घड़ा भरता है, उसे ऊपर खींचा जाता है। वह फिर टकराता है लेकिन घड़े की कोशिश है कि कम-से-कम छलके। अपनी तमाम व्यथा-कथा कहने के बाद भरा हुआ घड़ा प्रसन्न भाव से अब कुएं की जगत पर है। इस कविता के सस्वर, अभिनय पाठ पर खूब तालियां बजीं। सभी शिक्षकों ने गलदश्रु होकर सराहा। कुछ था जिसे बहुत खामोशी के साथ भीतर रौंप दिया गया था–अपनी सम्पूर्ण चेतना, भाव, ध्वनियों और नीयत के साथ। सोचता हूँ क्या शिक्षक भी ‘कुटिल कंकड़ों’की तरह नहीं होते जो हमें मांज-मांज कर, दीवारों से टकरा-टकरा कर हमें कुएं से निर्मल जल भर लेने का संदेश देते हैं। ऐसे ही थे मोतीलाल जैन और डी.एस. नागर। जब कक्षा में ‘उसने कहा था’ कहानी को पढ़ाते समय कोई शिक्षक कक्षा में फूट-फूट कर रोने लगे तो संवेदना के संस्कारों को अपने भीतर समाने से कैसे रोका जा सकता है ?
पिता डॉ. विश्वनाथ श्रोत्रिय शिक्षक थे। हमारे सामने ही उन्होंने उच्च स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण की। जब वे हिन्दी में एम.ए. कर रहे थे तो सुबह 4 बजे उठ कर महादेवी वर्मा की पंक्तियां सस्वर दुहराते– “ओ नभ की दीपावलियों तुम पल भर को बुझ जाना । मेरे प्रियतम को भाता है तम के परदे में आना।” हम अपनी अर्धनिद्रा में ये पंक्तियां सुनते। हालांकि उस समय न नभ का पता न प्रियतम और तम का, लेकिन कुल मिला कर यह सब सुनना अच्छा लगता। आलोचक रमेशचन्द्र शाह की मशहूर किताब ‘छायावाद की प्रासंगिकता’ को पढ़ने से पहले मेरे लिये छायावाद की प्रासंगिकता यही थी।
उज्जैन अनेक विभूतियों का शहर रहा है। पाण्डित्य और शोध् की एक अज़ीब-सी सुगंध यहाँ के पर्यावरण में बसी हुई है। पं. सूर्यनारायण व्यास, डॉ. शिवमंगलसिंह सुमन, डॉ. भगवतशरण उपाध्याय जैसी विभूतियों को मैंने स्वयं देखा है जिन्होंने इस धार्मिक नगरी को देश का ऐसा नगर बना दिया था जो विद्वत्ता का एक ऊर्जा केन्द्र था। एक ऐसा केन्द्र जिसके हस्तक्षेप के बगैर आप किसी रचनात्मक अनुष्ठान की पूर्णाहुति नहीं कर सकते। सुमनजी का ऐन्द्रजालिक व्यक्तित्व। हर जगह झूम रहे हैं –एक रचनात्मक ऊर्जा से भरे। ‘सौ सौ सुमन मिटें पर जिये अवन्ती नगरी’। उन दिनों सम्भावनाशील युवा कवि सुभाष दशोत्तर की अकाल मृत्यु ने सभी को चौंका दिया था। उनकी बहन जागृति हमारी सीनियर हुआ करती थी। तब तक कविता छायावाद से बरास्ता श्याम परमार, कौशल मिश्र, प्रमोद त्रिवेदी और सुभाष दशोत्तर होकर एक नई शक्ल बनाने लगी थी।
प्रेमचन्द पीठ पर शमशेर का आना उन दिनों की सबसे सुखद घटना थी। वे यूनिवर्सिटी कैम्पस में रहते थे। मैं उन दिनों एम.एस-सी. कर रहा था। डिपार्टमेन्ट जाते समय उनका घर रास्ते में पड़ता। मैं अक्सर घर से थोड़ा जल्दी निकल कर उनके पास बैठता। आँखों पर मायनस 22 का चश्मा…लेकिन आँखों में तैरती आत्मीयता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती। मुझ जैसे विद्यार्थी ;वह भी साहित्य का नहीं, की बात भी वे बहुत ध्यानपूर्वक सुनते। उनकी कविताओं को समझना आसान नहीं था लेकिन फिर भी उनसे यूं ही बतियाना काफी अच्छा लगता। इसके बाद उस पीठ पर नरेश मेहता, मन्नू भण्डारी, हरि नारायण व्यास आए। उनसे भी मुलाकातें हुई । बड़े रचनाकार से हर भेंट आपको भीतर से समृद्ध करती हैं। इन दिनों चन्द्रकान्त देवताले वहाँ हैं। बस, दुःख सालता है तो सिर्फ यह कि इतनी विभूतियों के संस्पर्श के बाद भी उज्जैन अपने भीतर साहित्य के गहन संस्कार नहीं पैदा कर पाया। कोई बड़ा कवि उज्जैन ने अपने परिवेश से पैदा किया हो, ऐसी सूचना न होना कितना बड़ा शून्य और अवसाद पैदा करती है ? क्या धोती-तिलक धारी पंडों की आपसी भांय-भांय ही किसी सर्जनात्मक परिवेश का पता देती है ? ऐसे ही कुछ कारण रहे होंगे जब मुक्तिबोध के भीतर दिल्ली और उज्जैन का संशय जागा होगा। वरना उज्जैन तो चुना ही जाना था।
इधर दिसम्बर शुरू हुआ और उज्जैन का आकाश पतंगों से भरने लगा। लाल,पीली,नीली,सफेद…..कागज के चौकोर परिन्दे आकाश को ढंक लेते हैं। इन परिन्दों की उड़ान की डोर छतों पर चढ़े।
आनन्द और उत्तेजना में चहकते पतंगबाजों के हाथों में होती है। पतंगबाजी का समूचा क्रम बहुत व्यवस्थित बाकायदा कांच पीस कर सरेस के साथ मंजा सूता जाता, सुखाया जाता, लपेटा जाता और फिर उसकी धार की जांच..‘..काटा है..’ की सामूहिक विजयी गर्जना…..। नीचे से आवाज़ें लग रही हैं….खाना ठंडा हो रहा है….बस… आते हैं अभी ..एक पेंच और। उज्जैन की छतों पर दिसम्बर की सुहानी धूप छितरी हुई है…ये छतें परस्पर संवाद की केन्द्र बनी हुई हैं। युवतियां बाल सुखा रही हैं…
पतंग के बहाने थोड़ा- बहुत नैन-मटक्का… कालिदास यूं ही तो नहीं कह गये—-लोलापांगेर्यदिन रमसे लोचनेर्वंचितोसि।
उज्जैन याने उत्सव… जीवन को भरपूर जी लेने की उत्कंठा…बहाना कुछ भी हो सकता है… चाहे सावन में महाकाल की सवारी हो या गणेशोत्सव की धूमधाम, मुहर्रम के ताजिये हों या फिर नवरात्रि के गरबे…दशहरा…दीवाली…होली की गैर…मालीपुरा का रात भर चलता कवि सम्मेलन…और प्रगतिशील सुमन एक बार फिर । मानो रीतिकाल को उज्जैन में उतार देते हैं…टेपा सम्मेलन की खिलखिलाहट…हर विभूति अपने भीतर बैठे जोकर से सामना कर रही है…इस खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा……। हर बार बारह वर्षों की प्रतीक्षा के बाद …सिंहस्थ पर्व। लोगों का अभूतपूर्व जमावड़ा। अखाड़ों, साधु- संतों और श्रद्धालुओं का धर्मिक समागम। स्थानीय जनता की रुचि अधिक इसमें कि चलो नई सड़कें, कुछ पुल, कुछ भवन बन जायेंगे। प्रदूषण और जलाभाव की मारी क्षिप्रा मैया को जैसे-तैसे बाँध कर नदी का स्वरूप दिया जा रहा है। जय घोष के साथ शाही स्नान…. मानों समूचे देश के रास्ते केवल उज्जैन की ओर ही जा रहे हैं। सिंहस्थ बीतता है… एक विशाल पर्व के हादसा विहीन गुजर जाने का प्रशासकीय संतोष…उज्जैन के चेहरे पर तैरता है। अब खाली-खाली तम्बू…डेरा है…उड़ गई चिड़िया का बसेरा बचा है और बची है पर्व के दौरान घटिया निर्माण कार्यों की सरकारी जांच।
विक्रम विश्वविद्यालय… सैकड़ों एकड़ में फैला परिसर…कभी देश के चुनिन्दा शिक्षा-केन्द्रों में शुमार..विद्वान् और तिकड़मी दोनों किस्मों की भरतियां । गोटियां और रोटियां … । इन सभी के बीच फलती-फूलती और दम तोड़ती संस्कृति भी। विक्रम कीर्ति मंदिर, कालिदास अकादमी, सिंधिया ओरियन्टल इंस्टिट्यूट…। ओम पुरी और जी.पी. देशपाण्डे का नाटक ‘उद्ध्वस्त धर्मशाला’… मोहन राकेश का ‘छतरियां’, कमलेश्वर, शरद जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, कवि रामविलास शर्मा कितने नाम लें। सभी उज्जैन आते हैं, जाने के बाद बहुत सारा उज्जैन अपने साथ ले जाते हैं।
उन दिनों ‘नई दुनिया’ में प्रकाशित पत्र सम्पादक के नाम में एक नाम बहुत पढ़ने को आता था– संजीव गुप्ता, बड़नगर। हर पत्र अपनी एक अलग तरह लिये हुए। एक दिन आश्चर्य की तरह उससे मुलाकात हुईं। उसके पिता ने सेठीनगर में ही प्लॉट लिया था जहाँ मेरा घर है। दिली खुशी हुई कि वह मेरा मुहल्लेदार होगा। फिर वह संजीव क्षितिज के नाम से कविताएं लिखने लगा। वह हकलाता था लेकिन उसकी कविता नहीं—-‘बाँसुरी के स्वरों को मशीनों के नाम / गिरवी रख देने के बाद/ कुछ भी तो नहीं है मेरे पास/ कि मैं बाँध सकूं अपने जानवरों की जुबान/ जंगल की सूखी पत्तियों से।’ उससे काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। बाद में सुना कि वह कहीं पत्रकार हो गया है…बीस साल हो गये होंगे…… फिर नहीं मिला… तुम कहाँ हो संजीव!
प्रभाकर श्रोत्रिय, श्रीराम तिवारी, पंकज पाठक, रामराजेश मिश्र, प्रमोद गणपत्ये, अमिताभ मिश्र, अशोक वक्त, सत्येन्द्र और योगेन्द्र मुखिया, पिलकेन्द्र अरोरा, शांतिलाल जैन, अर्चना श्रीवास्तव ये ऐसी शख्सियतें हैं जिनके सहारे कोई भी जीवन आसानी से बुना जा सकता है। ये सब उज्जैन के हैं। कुछ जनपदीय व्यक्तित्व!अपने-अपने फ़न में माहिर। इनमें से कईयों से सालों से नहीं मिला….. लेकिन लगता है कि बस.. हाथ भर की दूरी पर हैं ये सब। कभी आधी रात को भी ज़रूरत पड़ी तो पुकार लूंगा। यदि संकोच किया तो एक आत्मीय लताड़ सुनूंगा– निरंजन! तुम्हें शर्म नहीं आती यह सोचते। एक अदृश्य वायवीय तार खिंचा हुआ है जो उज्जैन ने बुना है। अपने लोगों की परिभाषा और कैसी होती होगी ? बता दूं कि इस सूची में अंतिम नाम मेरी पत्नी का है।
इन तमाम आकर्षणों के बावजूद उज्जैन निरंतर अग्रगामी नहीं है। वहाँ एक ठहराव है… कुछ फुरसत और निर्विकार भाव वाला ठहराव…। यहाँ जन्म लिये बालक का भविष्य उज्ज्वल तो है लेकिन यहाँ नहीं कहीं | और… ऐसे कई प्रमाण हैं उज्जैन में संस्कारित करने की अद्भुत शक्ति है लेकिन विकास के नैरंतर्य को बनाये रखने वाले परिवेश की कमी है। यहाँ आप जन्म ले सकते हैं…अपने जीवन के उत्तरार्ध में आकर प्रेमपूर्वक बस सकते हैं….. लेकिन कर्मजीवन….? क्या इसका कारण पचास किलोमीटर दूर बसा ‘मुम्बई का बच्चा’ इंदौर है… एक वटवृक्ष…?
उज्जैन के बारे में सोचते हुए भावुक हो जाता हूँ। फिर सोचता हूँ यह मेरे साथ ही तो नहीं है। हर कोई ऐसा ही करता होगा। एक नॉस्टेल्जिया हर व्यक्ति के भीतर होता ही है। जो बातें उज्जैन के बारे में है वह इस देश के किसी भी कस्बे या शहर की हो सकती हैं। ऐसे लोग देश के कोने-कोने में छितरे हुए हैं। क्या वे मेरे अपने लोग नहीं हैं ? इस देश की जनपदीय संरचना में एक अद्भुत आंतरिक साम्य है। उनके बाह्य रूप भिन्न हो सकते हैं। फिर उज्जैन ही क्यों ? भोपाल में राजेश जोशी और हरि भटनागर क्यों नहीं ? दिल्ली में उदय प्रकाश और मंगलेश डबराल क्यों नहीं ? नागपुर में बसन्त त्रिपाठी और मनोज रूपड़ा क्यों नहीं ? ऐसी अनेक जगहें और अनेक लोग क्यों नहीं ?
निरंजन श्रोत्रिय (निबंध-संग्रह ‘आगदार तीली’ से)